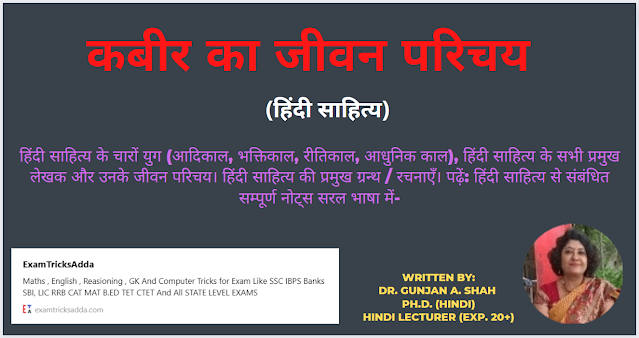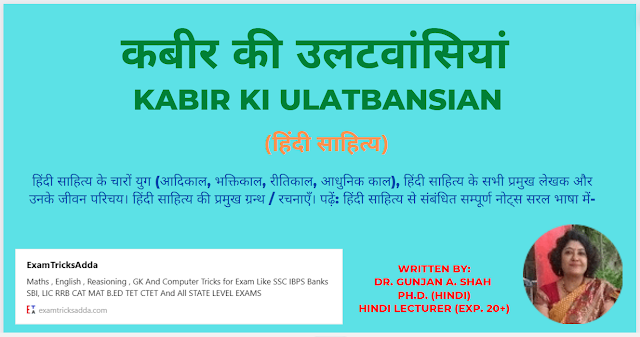संत काव्य | Sant Kavya
हिंदी साहित्य के भक्ति काल में दो धाराएं प्रवाहित हुई-
१. सगुण साहित्य
२. निर्गुण साहित्य
सगुण और निर्गुण साहित्य सम्बन्धी कुछ विशेष बिंदु
- सगुण काव्यधारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया राम काव्य धारा तथा कृष्ण काव्य धारा।
- निर्गुण काव्य धारा को दो शाखाओं में विभाजित किया गया संत काव्य धारा तथा सूफी काव्य धारा।
- संत काव्य धारा को ज्ञानमार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुणधारा के संत काव्य का नाम 'निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा' दिया है।
- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 'निर्गुण भक्ति साहित्य' कहते हैं ।
- रामकुमार वर्मा ने संत काव्य नाम दिया है जो अपेक्षाकृत अधिक संगत है।
संत शब्द का अर्थ
'संत' शब्द संस्कृत की धातु ' सद् ' से बना है और कई प्रकार से प्रयोग हुआ है (सत्य, वास्तविक, ईमानदार, सही)। इसका मूल अर्थ है 'सत्य जानने वाला' या 'जिसने अंतिम सत्य अनुभव कर लिया हो।'
'संत' शब्द से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने सत परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो। साधारण रूप में ईश्वरोन्मुख किसी भी सज्जन को और संकुचित रूप में निर्गुणोपासक भक्त को संत कहते हैं।
परशुराम चतुर्वेदी के मत में -
" संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है, जिसने सतरूपी परमतत्व का अनुभव कर लिया हो ।"
इस प्रकार जो सत्य का साक्षात्कार कर चुका हो, वही संत है। हिंदी साहित्य में कबीर, दादूदयाल, रैदास, नानक, और सुंदरदास आदि के काव्य को संत काव्य माना जाता है। संतकाव्य परंपरा १२ वीं सदी से आज तक चलती आई है। लेकिन धीरे-धीरे इसका काव्य पिष्टपेषित होने के कारण महत्वहीन होता गया । मध्ययुग की समाप्ति तक अपनी रूढ़िवादिता के कारण इसकी क्रांतिकारी भावना समाप्त हो गई । कबीर इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं।
संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं | प्रवृत्तियाँ | Sant Kavya ki Pravritiyan
संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदायों के तत्वों का समन्वय है, लेकिन संतो ने धर्म अथवा साधना की शास्त्रीय ढंग से परिभाषा नहीं दी। संत साधु पहले थे और कवि बाद में । संत काव्य की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
(१) निर्गुण ईश्वर में विश्वास
संत कवियों ने अपने काव्य में निर्गुण ईश्वर में विश्वास और कुछ सीमा तक सगुण रूप का विरोध किया है। कबीर का कथन है-
" दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना ।
राम नाम का मरम है आना । "
संत निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं जो घट -घट में वास करता है। इनके ईश्वर का न तो कोई रंग है, न रूप है, न जाति है ,न कोई आकर है, न वह जन्म लेता है और न ही वह मर सकता है, वह तो अजर -अमर है , आगोचर है ,निराकार है ,निर्गुण है ,शाश्वत है ।सभी वर्णो एवं जातियों के लिए वह निर्गुण ही उपास्य है।
" निर्गुण राम जपहु रे भाई ?
अविगत की गति लिखी न जाई ।"
(२) बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध
संतो ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद की भावना का खंडन किया है। इसका कारण, शंकर मत का प्रभाव तथा तत्कालीन मुसलमान शासकों का एकेश्वरवादी होना था । हिंदू -मुस्लिम एकता के लिए संतों ने एकेश्वरवाद का संदेश सुनाया ।
कबीर कहते हैं -
"अक्षर पुरुष इक पेड़ है, निरंजन वाकी डार ।
त्रिदेवा शाखा भये, पात भया संसार। "
वस्तुत: संतो की उपासना का लक्ष्य सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। फिर भी सगुन उपासकों की भांति उन्होंने अपने प्रियतम को राम, कृष्ण ,गोविंद, केशव आदि नामों से पुकारा है।
(३) गुरु का महत्व
संत काव्य के सभी कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसे ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है क्योंकि ईश्वर तक पहुंचाने वाला गुरु ही है। गुरु ही ज्ञान के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है ।
कबीर कहते हैं-
" गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागूं पांय।
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया ।"
संत कवियों का विश्वासहै कि राम की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है ।कबीर कहते हैं -
" गुरु धोबी सिस का कपड़ा, साबुन
सिरजनहार।
सूरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति
अपार ।"
अर्थात् गुरु धोबी के समान है, शिष्य कपड़े के समान है और प्रभु उस साबुन के समान है जिसके प्रयोग से कपड़ा साफ होता है ।इस प्रकार गुरु कृपा के बिना शिष्य में ज्ञान का विकास संभव नहीं है।